आत्मकथा
“मेरी कलम मेरा संघर्ष”
लेखक: जयप्रकाश रावत
प्रस्तावना
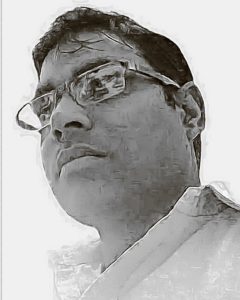
हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ लम्हें ऐसे होते हैं जो उसे हमेशा के लिए बदल देते हैं। मेरे जीवन में भी कई मोड़ आए — कुछ ने मुझे तोड़ा, तो कुछ ने मुझे नया आकार दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक गाँव का लड़का, जो खेतों की मेड़ पर दौड़ता था, वो एक दिन पत्रकारिता की दुनिया में अपनी पहचान बना पाएगा।
मैंने पत्रकारिता को कभी सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रखा। मेरे लिए यह ज़रिया था — उन आवाज़ों तक पहुँचने का जिन्हें समाज ने अनसुना कर दिया था। संदेश महल की स्थापना हो, या स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को खोजने की मेरी कोशिश — हर पहल ने मुझे एक नई दृष्टि दी, एक नई जिम्मेदारी सौंपी।
यह आत्मकथा मेरा खुद से संवाद है — और उन लोगों से भी, जिन्होंने मेरे शब्दों में अपने जीवन की छवि देखी है।
जयप्रकाश रावत
भूमिका
हर जीवन एक यात्रा है—कभी शांत तो कभी तूफानी। यह यात्रा केवल साँसों की गिनती नहीं, बल्कि अनुभवों का गहन दस्तावेज़ होती है। मेरी यह आत्मकथा, न तो किसी महापुरुष की गाथा है, न ही किसी आदर्श चरित्र की कथा। यह एक साधारण व्यक्ति की असाधारण जिजीविषा की कहानी है—जो अपनी मिट्टी से जुड़ा रहा, और समय के साथ अपने विचारों, संघर्षों, और सपनों की शृंखला को शब्दों में पिरोता चला गया।
मैंने जीवन को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि जिया है—हर मोड़ पर कुछ सीखा, कभी अपनों से, कभी अजनबियों से, और अक्सर हालातों से। पत्रकारिता, लेखन और समाजसेवा—ये मेरे जीवन के ऐसे तीन आयाम हैं, जिनमें मैंने खुद को हर बार नए रूप में पाया।
इस आत्मकथा का उद्देश्य आत्मप्रशंसा नहीं, आत्मविश्लेषण है। यह उन अनसुने किस्सों की पुकार है जो अक्सर इतिहास के हाशिए पर छूट जाते हैं। यह उन चेहरों की पहचान है, जिनका योगदान अनगिनत दिलों में तो है, पर कागज़ों पर दर्ज नहीं।
मैं चाहता हूँ कि मेरी यह जीवनगाथा केवल पढ़ी न जाए, बल्कि महसूस की जाए—शब्दों के उस स्पर्श के साथ, जो दिल तक पहुँचता है। यदि इस आत्मकथा की कोई भी पंक्ति आपको सोचने, मुस्कुराने या प्रेरित होने के लिए मजबूर करे, तो समझूँगा कि मेरा प्रयास सफल रहा।
आपका —
जयप्रकाश रावत
समर्पण
यह आत्मकथा मैं समर्पित करता हूँ—
उन जड़ों को, जहाँ से मेरा अस्तित्व फूटा,
उन शाखाओं को, जिन्होंने मुझे विस्तार दिया,
और उन फूलों को, जिनसे मेरी यात्रा महकती रही।
सबसे पहले—मेरे माता-पिता को, जिनके संस्कारों ने मुझे ज़मीन से जोड़े रखा, और जिनके आशीर्वादों की छाया में मैं हर तूफ़ान को पार कर सका।
मेरी जीवनसंगिनी को, जिसने हर मोड़ पर मेरी भावनाओं को समझा, मेरे मौन को सुना, और मेरी व्यस्तताओं में भी साथ निभाया। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने मुझे कभी थकने नहीं दिया।
उन गुरुओं को, जिन्होंने मुझे केवल पढ़ाया नहीं, बल्कि जीवन को देखने की दृष्टि दी। आपकी सीखें मेरी आत्मा की रोशनी बनीं।
उन तमाम साथियों, संपादकों, लेखकों और पाठकों को, जिनके सहयोग, आलोचना और प्रोत्साहन ने मुझे बेहतर बनने का साहस दिया।
और अंततः, उस भारत माता को—जिसकी मिट्टी में मैं जन्मा, जिसकी भाषा में मैंने सोचा और लिखा, और जिसके समाज के लिए मैंने कलम और कर्म दोनों समर्पित किए।
यह आत्मकथा किसी एक व्यक्ति की नहीं, उन सभी का साझा प्रतिबिंब है जिन्होंने किसी न किसी रूप में मुझे गढ़ा है।
जयप्रकाश रावत
दो शब्द
प्रिय पाठकों,
आपके हाथों में जो पुस्तक है, वह केवल एक जीवन की दास्तान नहीं, बल्कि विचारों की वह यात्रा है, जो संघर्ष, विश्वास और सामाजिक चेतना की पगडंडियों से होकर गुज़री है।
मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने ही जीवन को शब्दों में बाँधना इतना कठिन होगा। हर स्मृति के साथ कोई भावना जुड़ी थी—कहीं पीड़ा, कहीं संतोष, कहीं मुस्कान, तो कहीं आंखों की नमी। इस आत्मकथा को लिखते हुए ऐसा लगा जैसे मैं बार-बार अपने अतीत से होकर गुजर रहा हूँ—हर बार कुछ नया समझते हुए, कुछ पुराना छोड़ते हुए।
यह पुस्तक उन युवाओं के लिए भी है, जो सीमित संसाधनों में असीम सपने देखते हैं। उनके लिए, जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ना चाहते हैं, पर दिशा की तलाश में भटकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा अनुभव उनके लिए एक दीपक बने—जो भले ही छोटा हो, लेकिन रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखता हो।
यह आत्मकथा कोई पूर्णता का दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि एक प्रयास है—खुद को समझने का, और समाज के सामने एक ईमानदार चित्र प्रस्तुत करने का। यदि इस लेखनी में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, तो वह मेरी मानवीय सीमा है, मेरा अभिमान नहीं।
आपके हाथों में यह पुस्तक मेरी ज़िंदगी की नब्ज़ है। इसे पढ़ते समय अगर आप मेरे साथ चलें, मेरे साथ महसूस करें, तो यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।
सादर,
जयप्रकाश रावत
(लेखक, पत्रकार, समाजसेवक)
अध्याय 1
– मेरा जन्म और आरंभिक जीवन
(पृष्ठ संख्या – 1)
3 मई 1982 — यह वही दिन था जब मैंने पहली बार इस संसार की साँसें लीं। एक साधारण-से गाँव बिबियापुर, जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में पड़ता है, वहीं मेरी पहली किलकारी गूंजी।पोस्ट रूहेरा, तहसील सूरतगंज का यह इलाक़ा, भले ही नगरों की चकाचौंध से दूर रहा हो, पर वहां की मिट्टी में अपनापन था, रिश्तों की खुशबू थी और सपनों की सादगी थी।
मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा जहाँ जीवन साधनों में सीमित था, पर स्नेह और संस्कारों की कोई कमी न थी। मेरे माता-पिता ने कभी बड़ी बातें नहीं कीं, पर उनका जीवन ही मेरे लिए सबसे बड़ी सीख बना। माँ की ममता और पिता की मेहनत — इन दोनों के मेल ने मेरे अंदर आत्मबल का बीज बोया।
बचपन मेरे लिए पेड़ की छांव, कच्चे रास्तों, तालाबों की लहरों और मिट्टी की सौंधी खुशबू में बीता। स्कूल तक पैदल जाना, बस्ते में किताबों से ज़्यादा सपनों का बोझ, और आंखों में कुछ ऐसा कर गुज़रने की ललक — यही मेरी आरंभिक दुनिया थी।
तब न तो मोबाइल था, न इंटरनेट। मनोरंजन का माध्यम कोई स्क्रीन नहीं, बल्कि गाँव के बुज़ुर्गों की कहानियाँ होती थीं। उन्हीं से मैंने स्वतंत्रता संग्राम के किस्से सुने, देशभक्ति की पहली चिंगारी वहीं से मेरे भीतर सुलगी।
एक छोटे से गाँव में जन्म लेकर बड़ा सपना देखना आसान नहीं था। लेकिन मैंने बचपन से ही ठान लिया था कि अपनी पहचान बनानी है — सिर्फ़ अपने लिए नहीं, बल्कि उस समाज के लिए, जो हर दिन संघर्ष करता है, पर जिसकी कहानियाँ कोई नहीं सुनता।
यहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई — एक साधारण बालक से एक सचेत पत्रकार, समाजसेवी और लेखक बनने की ओर…
अध्याय 2 –
शिक्षा और सोच का विस्तार
(पृष्ठ संख्या – 5)
बिबियापुर की माटी में जन्मा सपना
(एक गाँव, एक बच्चा और अनकहा संघर्ष)
बिबियापुर — उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में बसा एक छोटा सा गाँव, जो मानचित्र पर भले ही एक बिंदु हो, लेकिन मेरे लिए यह मेरी जड़ों की पवित्र भूमि है। यहीं मैंने पहली बार जीवन को खुली आँखों से देखा, यहीं पहली बार धूप की तपिश और संघर्ष की सच्चाई को महसूस किया।
मेरी शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक विद्यालय तेलवाय से हुई, पर विद्यालय का खुद का भवन न था। इसलिए गाँव के पंचायत भवन की दीवारें ही हमारी कक्षा बन गईं। जब छत टपकती थी तो हम अपनी स्लेटों को किताबों पर रख लेते, और जब ज़मीन कीचड़ से भर जाती, तो हम नंगे पाँव ही ज्ञान की राह पर आगे बढ़ते।
हमारे शिक्षक — श्री रामनाथ वर्मा और श्री रामचंद्र वर्मा, सच्चे गुरु थे। वे पढ़ाते ही नहीं थे, जीवन का मार्ग भी दिखाते थे। उनका स्नेह और अनुशासन मेरे जीवन के स्थायी स्तंभ बन गए।
जब मैं कक्षा पाँच में उत्तीर्ण हुआ, तो मेरी मेहनत का प्रतिफल मिला — वजीफे की छोटी-सी धनराशि। उसी से मेरी माँ और पिता जी ने मेरे लिए सिलवाई थी सफेद शर्ट और काली पैंट।
मैंने पहली बार ऐसा पहनावा पहना था जो किसी आम दिन से अलग था। उस दिन आईने में खुद को देखते हुए मुझे पहली बार विश्वास हुआ कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ।
हालाँकि पैरों में चप्पल नहीं थीं, लेकिन उस दिन मेरे पाँव धरती पर नहीं, सपनों पर चल रहे थे। मेरे नंगे पाँवों में गाँव की धूल थी, पर मन में था आत्मसम्मान का झरना।
वह पोशाक सिर्फ कपड़े नहीं थे — वे मेरे पहले सपने का रूपांतरण थे।
एक किसान की झोंपड़ी में जन्मा लड़का, जो खेतों के बीच खेलता था, अब धीरे-धीरे कलम की दिशा में बढ़ने लगा था।
आज जब मैं उस पल को याद करता हूँ, तो आंखें नम हो जाती हैं। बिबियापुर की वह माटी आज भी मेरी लेखनी में महकती है।
यही मेरी शुरुआत थी — और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी।
मेरे शिक्षकों ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। उन्होंने केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया, बल्कि आत्मा को जगाया। यही कारण था कि मैं हर विषय में केवल उत्तर खोजने से ज़्यादा प्रश्न करने की ललक लेकर आगे बढ़ता गया।
यह अध्याय मेरी ज़िंदगी का वह आधार है, जिस पर आगे चलकर पत्रकारिता, लेखन और समाजसेवा की पूरी इमारत खड़ी हुई।
अध्याय 3 –
पत्रकारिता में पहला कदम
(पृष्ठ संख्या – 9)
कॉलेज के दिनों में जहाँ अधिकांश छात्र अपने भविष्य को लेकर भ्रम में रहते थे, वहीं मेरे भीतर एक अलक्षित-सी स्पष्टता पनप रही थी—मुझे लिखना है, बोलना है, और सबसे बढ़कर—समाज के लिए कुछ करना है।
पत्रकारिता मेरे लिए कोई पेशा नहीं थी, बल्कि एक मिशन की तरह थी। पहली बार जब मैंने अख़बार में ‘जनहित’ से जुड़ी एक रिपोर्ट पढ़ी, तो मेरे भीतर हलचल हुई। मैंने महसूस किया कि एक छोटी सी खबर भी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। बस यहीं से कलम थामने की शुरुआत हुई।
कॉलेज की दीवार पत्रिकाओं में मैंने लेख लिखने शुरू किए। शुरुआत में शायद ही किसी ने गौर किया, लेकिन मेरे शब्दों में सच्चाई थी—और वह सच्चाई धीरे-धीरे ध्यान खींचने लगी। मेरा पहला प्रकाशित लेख स्थानीय समस्याओं पर था, जो एक छोटे से अख़बार में छपा। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी बात अब सिर्फ़ डायरी तक सीमित नहीं रही।
इसके बाद मैंने हिन्दी दैनिक आज,राष्ट्रीय सहारा, पंजाब केसरी जैसे प्रमुख समाचारपत्रों में फ्रीलांस लेखन किया। मेरे लेखों की खासियत थी—जमीनी मुद्दों की पकड़ और मानवीय संवेदनाओं की झलक। मैं सिर्फ खबर नहीं लिखता था, मैं उन चेहरों को शब्द देता था जो अकसर समाज में अनसुने रह जाते हैं।
प्रेस की दुनिया में प्रवेश करना आसान नहीं था। न कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि, न कोई राजनीतिक रसूख। सिर्फ़ मेहनत थी, और अपने विषयों के प्रति ईमानदारी। कई बार मेरी खबरें छपने से रोकी गईं, कई बार दबाव डाले गए, लेकिन मैंने कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा।
पत्रकारिता ने मुझे एक नई दृष्टि दी—देखने, सुनने, समझने और फिर उसे समाज तक पहुँचाने की। मैंने महसूस किया कि कलम की ताक़त बंदूक से कहीं ज़्यादा है—यह किसी को गिरा नहीं सकती, लेकिन किसी को उठा ज़रूर सकती है।
इसी दौरान एक विचार मन में अंकुरित हुआ—क्यों न अपना खुद का मंच हो? एक ऐसा माध्यम जहाँ सिर्फ सच्चाई की गूंज हो, न कि सत्ता और विज्ञापन का दबाव!
यह विचार आने वाले अध्याय की नींव बन गया—“संदेश महल” की।
अध्याय 4 –
संदेश महल की स्थापना
(पृष्ठ संख्या – 13)
जब पत्रकारिता की दुनिया में कुछ वर्ष बिताए, तो यह एहसास गहराता चला गया कि मुख्यधारा के मीडिया में कहीं न कहीं जनसरोकार खोते जा रहे हैं। समाचार अब एक व्यापार बनता जा रहा था, जहाँ TRP, विज्ञापन और एजेंडा—सच की जगह लेने लगे थे।
मैंने कई बार महसूस किया कि जिन आवाज़ों को सबसे ज़्यादा सुनाए जाने की ज़रूरत थी, वही आवाज़ें सबसे ज़्यादा दबा दी जाती थीं। उस समय मन में एक ही सवाल गूंजता था—क्या यही पत्रकारिता है? क्या हमारा दायित्व बस यही है कि जो बिके वही दिखे?
इन्हीं प्रश्नों ने एक नई दिशा दिखाई। मैंने निर्णय लिया—अपना मंच शुरू करूंगा। एक ऐसा मंच, जहाँ न डर होगा, न दबाव; जहाँ सच्चाई को जगह मिलेगी और ज़मीन से जुड़ी पत्रकारिता को नया जीवन मिलेगा।
और यहीं से जन्म हुआ — “संदेश महल” का।
संदेश महल का प्रारंभ एक छोटे से डिजिटल पोर्टल से हुआ। शुरुआत में न कोई बड़ी टीम थी, न कोई बड़ा संसाधन। बस थी तो एक सच्ची लगन, और कलम पर अटूट विश्वास। मैंने इसे दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रूप में विकसित किया—हर वर्ग के पाठकों के लिए कुछ न कुछ।
शुरूआती दिनों में ख़ूब संघर्ष हुआ। तकनीकी ज्ञान सीमित था, संसाधन भी नहीं थे। कभी नेटवर्क नहीं चलता, कभी साइट हैंग हो जाती, लेकिन एक बात स्पष्ट थी—झुकना नहीं है।
धीरे-धीरे पाठकों ने ध्यान देना शुरू किया। हमारे लेखों, रिपोर्टों और विश्लेषणों में जो ईमानदारी थी, वह लोगों को छूने लगी।
संदेश महल सिर्फ एक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म नहीं रहा, वह एक आंदोलन बन गया। एक ऐसा आंदोलन, जो छोटे पत्रकारों को, ग्रामीण संवाददाताओं को, युवाओं को और सामाजिक मुद्दों को एक मंच देने लगा। हमनें उन चेहरों को स्थान दिया, जो सालों से अनदेखे रह गए थे—स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, लोक कलाकार, शिक्षक, किसान।
मेरी भूमिका एक संपादक से कहीं बढ़कर थी—मैं प्रकाशक भी था, संवाददाता भी, तकनीकी सहायक भी और मार्गदर्शक भी। हर समाचार, हर विशेषांक, हर पंक्ति में मेरी आत्मा झलकती थी।
आज जब मैं www.sandeshmahal.com को देखता हूँ, तो गर्व होता है कि यह केवल एक वेबसाइट नहीं, यह मेरे जीवन दर्शन का प्रतिबिंब है। यह मंच उन विचारों का महल है, जिनकी नींव सत्य, संवेदना और सरोकार पर रखी गई है।
अध्याय 5
ह्यूमन वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट: सेवा का दूसरा नाम
(पृष्ठ संख्या – 17)
पत्रकारिता के माध्यम से समाज की समस्याओं को उजागर करते हुए एक बात बार-बार मन को खटकती थी—क्या केवल खबरें प्रकाशित कर देना ही पर्याप्त है?
जब तक कोई ठोस कार्रवाई न हो, तब तक बदलाव अधूरा रहता है। यही सोच मुझे सेवा की दिशा में ले गई।
सालों तक मैंने देखा—किसी गाँव में बीमार बुज़ुर्ग दवा के लिए तरस रहे हैं, किसी विधवा को पेंशन नहीं मिल रही, किसी मेधावी छात्र को फीस भरने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। मन विचलित होता था। आखिर निर्णय लिया—अब कुछ करना होगा, और सिर्फ़ कलम से नहीं, कर्म से।यहीं से जन्म हुआ—ह्यूमन वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का।
इस ट्रस्ट की स्थापना एक बहुत ही सरल और स्पष्ट उद्देश्य के साथ की गई—हर उस जरूरतमंद तक पहुँचना, जिसे सिस्टम ने भुला दिया है।
चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा, रोजगार, या सामाजिक न्याय—हमने हर दिशा में काम करने का संकल्प लिया।
मैंने इस ट्रस्ट को कोई नाम के लिए नहीं, बल्कि आत्मा से चलाया। दिन-रात बिना थके हमनें लोगों तक राहत पहुँचाई—कभी अनाज के पैकेट, कभी कंबल, कभी दवा, और कभी कानूनी मदद।कोरोना काल के समय जब सब ठहर गए थे, तब हमने गाँव-गाँव पहुँचकर लोगों को मदद दी। यही वो क्षण थे जब लोगों ने केवल हमारे ट्रस्ट को नहीं, बल्कि विश्वास को महसूस किया।
मुझे गर्व है कि आज ट्रस्ट के माध्यम से न केवल सहायता दी जाती है, बल्कि सम्मान भी। हम उन बुज़ुर्ग स्वतंत्रता सेनानियों को मंच देते हैं, जिनके योगदान को भुला दिया गया था। हम बच्चों को किताबें देते हैं, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हैं, युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं।
आज मैं जब ट्रस्ट के किसी आयोजन में खड़ा होता हूँ, और देखता हूँ कि किसी की आँखों में उम्मीद की चमक लौट आई है—तो वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है।
सेवा मेरे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जीवन की आंतरिक आवश्यकता है। और शायद यही कारण है कि पत्रकारिता और सेवा—दोनों मेरे जीवन के दो पहलू हैं, जो एक-दूसरे को पूर्ण करते हैं।
अध्याय 6
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की खोज और लेखनी से पुनर्जीवन
(पृष्ठ संख्या – 21)
जब मैंने पत्रकारिता और सेवा के क्षेत्र में क़दम मज़बूती से रख लिए, तब एक और आवाज़ मेरे अंतर्मन को पुकारने लगी—उन नायकों की, जिनकी गाथाएँ समय की धूल में दब गई थीं।
स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ बचपन से सुनता आया था। पर जैसे-जैसे बड़ा हुआ, यह महसूस किया कि इतिहास की मुख्यधारा में सिर्फ़ कुछ चुनिंदा नामों का ही उल्लेख मिलता है। गाँव-गाँव, तहसील-तहसील में ऐसे असंख्य सपूत थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, पर न उनकी तस्वीरें हैं, न कोई स्मृति।
मेरे मन ने कहा—अगर मैं पत्रकार हूँ, लेखक हूँ, तो मेरी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इन भूले-बिसरे नायकों को फिर से जीवित करूँ—शब्दों में, स्मृतियों में और समाज की चेतना में।
मैंने गाँव-गाँव जाकर खोज शुरू की। कभी किसी बुज़ुर्ग से सुनी बातों का पीछा किया, कभी पुराने अभिलेखागारों की धूल फाँकी, कभी परिवारों से संपर्क किया, जो अब गुमनामी में जी रहे थे।
यही प्रयास मुझे लाकर खड़ा कर देते हैं उन नामों के आगे, जिन पर न देश ने ध्यान दिया और न व्यवस्था ने। जैसे—
राजा बलभद्र सिंह,
महन्त जगन्नाथ बक्स दास,
पंडित उमा शंकर मिश्र,
राम आसरे वर्मा,
रफी अहमद किदवई,
चंद्रशेखर तिवारी,
और अच्युतानंद नंद दीक्षित जैसे दर्जनों नाम।
इनके बारे में मैंने जितना जाना, उतना ही मेरा मन विनम्र होता गया।इन पर मैंने विशेष शोध लेख तैयार किए, जिनमें उनका योगदान उनका संघर्ष और उनका विस्मरण सब कुछ ईमानदारी से रखा गया।यह लेख विभिन्न समाचारपत्रों और संदेश महल में प्रकाशित हुए और पाठकों ने इन्हें हाथों-हाथ लिया।
कुछ परिवारों की आँखें नम हो गईं, जब उन्होंने पहली बार अपने पूर्वजों की गाथा अख़बार में देखी। मेरे लिए यही सम्मान का क्षण था—उनकी खोई हुई पहचान को लौटा पाना।
मैंने महसूस किया कि इतिहास केवल अतीत नहीं होता, वह भविष्य की नींव होता है। अगर हम अपने असली नायकों को नहीं पहचानते, तो आने वाली पीढ़ियाँ केवल अधूरी तस्वीरों से प्रेरणा लेंगी।
आज भी यह कार्य मेरी प्राथमिकताओं में है। जब तक कलम चलेगी, तब तक मैं उस मिट्टी के सपूतों को लिखता रहूँगा, जिनकी तपस्या के बिना आज हमारा यह स्वतंत्र जीवन अधूरा होता।
अध्याय 7
साहित्यिक रचनाएँ और अप्रकाशित कृतियाँ
(पृष्ठ संख्या – 26)
पत्रकारिता और समाजसेवा के बीच जीवन एक दिशा में बहता रहा, पर मन का एक कोना हमेशा रचनात्मकता के रंग में भीगता रहा। ख़बरों की सख़्ती के पीछे एक संवेदनशील आत्मा हर वक़्त धड़कती रही—जिसे अभिव्यक्ति चाहिए थी, कभी कविता बनकर, कभी कहानी, कभी उपन्यास की शक्ल में।
मेरे लेखन की शुरुआत भले ही समाचारों से हुई हो, लेकिन साहित्यिक दुनिया में क़दम रखते ही एक नया संसार खुल गया।
भावनाएँ, विचार, अनुभव—सब कुछ अब शब्दों में ढलने लगे। मैं सिर्फ़ लिखता नहीं था, जीता था—हर पात्र, हर संवाद, हर एहसास को।मेरी पहली गंभीर रचना रही – “सविता”, एक अप्रकाशित उपन्यास, जो संत नारायण दास जी के जीवन, दर्शन और सामाजिक संघर्षों पर आधारित है।यह केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं, बल्कि एक कालखंड की कहानी है।इस उपन्यास को लिखते हुए मैंने केवल कलम नहीं चलाई, बल्कि अपने भीतर झाँका, अपने समाज को देखा और अपने विश्वासों को काग़ज़ पर उकेरा।
इसके अतिरिक्त, कई लेख व विशेषांक प्रकाशित हुए हैं —
विशेषकर “देवा महोत्सव पत्रिका” में संत नारायण दास पर लिखी गई मेरी रचना को पाठकों ने बहुत सराहा।धार्मिक-सांस्कृतिक संदर्भों को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ना, मेरे साहित्य का केंद्रीय भाव रहा है।मेरी कविताएँ अक्सर सामाजिक प्रश्नों से टकराती हैं—अन्याय,भेदभाव, शोषण, और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान के लिए जूझता आम इंसान।
इनमें न कोई बनावट है, न कोई दिखावा—सिर्फ़ एक सच्चा स्वर, जो पाठक के दिल में सीधे उतरता है।
हालाँकि अभी बहुत-सी रचनाएँ प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं, पर मेरे लिए साहित्य केवल छपने का माध्यम नहीं है—यह मेरी आत्मा की पुकार है।मैं जानता हूँ कि समय आएगा, जब ये शब्द किसी न किसी पाठक के जीवन में एक दीप की तरह जलेंगे।
आज भी जब रात गहराती है, और दुनिया सो जाती है—मेरे भीतर एक आवाज़ जागती है, जो कहती है—लिखो, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी के जीवन का सहारा बन सकते हैं।
अध्याय 8
सामाजिक सरोकारों से सीधा संवाद
(पृष्ठ संख्या – 31)
पत्रकारिता, साहित्य और सेवा—इन तीनों के केंद्र में अगर कुछ था, तो वह था समाज।
मेरा हर प्रयास, हर कदम, हर विचार इस भावना से प्रेरित था कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, और क्या बदल सकता हूँ।
मैंने कभी भी खुद को केवल “कलम का आदमी” नहीं माना। मेरी कलम तभी सशक्त रही जब वह जनता की पीड़ा से जुड़ी, जब वह वंचित की आवाज़ बनी।यही वजह रही कि मैंने कभी दफ़्तर में बैठकर समाज को देखने की कोशिश नहीं की—बल्कि मैं उस धूल भरे रास्ते पर चला जहाँ लोग रोज़ संघर्ष करते हैं।
बेसहारा विधवाओं, खेत में हल जोतते किसानों, दवा के लिए भटकते रोगियों, बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं और न्याय के लिए दर-दर भटकते लोगों की कहानियाँ मैंने केवल सुनी नहीं, जानी भी और जी भी।
मैंने कई बार ऐसे जन मुद्दों को उठाया जिन्हें बड़े मीडिया ने अनदेखा किया था।
कभी जल संकट पर रिपोर्ट बनाई, कभी शिक्षा के अधिकार की अनदेखी पर आंदोलन से जुड़ा, तो कभी दलितों पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध लेखनी को हथियार बनाया।
इन्हीं प्रयासों के दौरान मुझे समझ में आया कि सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं, बल्कि उस लिखे को लोगों के बीच संवाद का माध्यम बनाना भी ज़रूरी है।इसलिए मैंने जनचौपालों, ग्रामीण संवादों, युवा सभाओं और जनसुनवाइयों में भाग लेना शुरू किया। मैं चाहता था कि जनता भी बोले, और मैं सुन सकूँ।
संदेश महल इस संवाद का सशक्त मंच बनकर उभरा। वहाँ छपी हर खबर, हर विश्लेषण, हर विचार, समाज से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता।हमारे पाठकों में गाँव का किसान भी था, स्कूल की छात्रा भी, नगर का व्यापारी भी और बेरोजगार युवक भी।यही विविधता हमारे लेखन को ज़्यादा जीवंत और प्रभावशाली बनाती रही।
आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो पाता हूँ कि समाज से मेरा यह सीधा संवाद ही मेरी सबसे बड़ी पूँजी है।मैंने न तो मंचों पर भाषण दिए, न सत्ता के गलियारों में रिश्ता जोड़ा—मेरा रिश्ता बस एक ही था, जनता से, ज़मीन से, ज़रूरत से।
अध्याय 9
सम्मान, संघर्ष और मेरी पहचान
(पृष्ठ संख्या – 36)
हर रास्ता फूलों से नहीं सजा होता, और हर संघर्ष के बाद तालियाँ नहीं बजतीं।
मेरे जीवन में भी यह द्वंद्व बार-बार सामने आया एक ओर संघर्षों की कठोर आग, दूसरी ओर सम्मानों की ठंडी छाँव।
जब मैंने कलम उठाई थी, तब यह अंदाज़ा नहीं था कि एक सच्चाई को उजागर करना कितनों की आँखों में चुभ सकता है।कई बार धमकियाँ मिलीं, विरोध झेलना पड़ा, और कभी अपनों ने भी दूरी बना ली।पर मैंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, क्योंकि मैंने पत्रकारिता को साधन नहीं, साधना माना।
सत्ता के गलियारों में जगह नहीं मिली, लेकिन जनता के दिलों में जगह बनती गई।
जब किसी किसान ने कहा—“भाई, आपने हमारी बात छाप दी, अब अधिकारी सुनने लगे हैं।”या जब किसी छात्र ने कहा—“आपकी प्रेरणा से मैंने भी लिखना शुरू किया है।”
तो लगा, यही असली सम्मान है।
कुछ संस्थाओं ने आधिकारिक रूप से भी सम्मानित किया—पत्रकारिता, सामाजिक सेवा और साहित्यिक योगदान के लिए।
पर मैं उन गुमनाम प्रशंसाओं को ज़्यादा संजो कर रखता हूँ, जो चिट्ठियों, फोन कॉल्स या एक बुज़ुर्ग के आशीर्वाद के रूप में मिलीं।
मुझे आज भी याद है वो दिन, जब एक छोटे से गाँव में एक महिला आई और बोली—
“आपने मेरी बेटी की शिक्षा के लिए जो मदद की थी, आज वही लड़की टीचर बन गई है।”
उस पल मेरी आँखों में आँसू थे, लेकिन वो खुशी के थे, आत्मसंतोष के थे।
मेरी पहचान कभी भी किसी पद, पुरस्कार या प्रकाशन से नहीं बनी—वो बनी है सत्य के प्रति मेरी प्रतिबद्धता, जनता के प्रति मेरी निष्ठा और आत्मा की आवाज़ के प्रति मेरी ईमानदारी से।
आज जब लोग मुझे पहचानते हैं तो मैं सिर झुका कर कहता हूँ—यह पहचान मेरी नहीं, आप सबके विश्वास की है।
अध्याय 10
नया सपना, नई पीढ़ी और मेरी कलम की विरासत
(पृष्ठ संख्या – 41)
जब मैं आज की पीढ़ी को देखता हूँ—उनकी आँखों में चमक, ऊर्जा और संभावनाएँ—तो मन आश्वस्त होता है कि भविष्य उज्ज्वल है, बशर्ते वे अपनी जड़ों को न भूलें।
मेरी यात्रा जितनी व्यक्तिगत रही, उतनी ही यह समाज से जुड़ी भी रही है।
अब जब उम्र, अनुभव और आत्मबोध का एक संगम सामने है, तो यह जिम्मेदारी महसूस होती है कि जो मैंने सीखा, जिया और लिखा—वो अगली पीढ़ी तक पहुँचे।
मेरा सपना है कि संदेश महल सिर्फ एक पोर्टल न रहे, बल्कि एक आंदोलन बने—जहाँ नई पीढ़ी के पत्रकार, लेखक, समाजसेवी जुड़ें, और सच्चाई के साथ अपने विचार दुनिया तक पहुँचाएँ।
मैं चाहता हूँ कि बच्चे सच लिखने से न डरें, युवाओं के हाथ में सिर्फ़ मोबाइल न हो, बल्कि विचार हो, सवाल हों, और समझदारी हो।
मैं देखता हूँ कि शब्दों की ताक़त आज भी सबसे बड़ी है—और अगर सही दिशा में चले तो ये क्रांति भी ला सकते हैं।
अब मेरा लेखन सिर्फ़ प्रकाशित पंक्तियाँ नहीं, बल्कि विरासत बन चुका है।
वो विरासत, जिसे मैं अगली पीढ़ी को सौंपना चाहता हूँ—
वो ईमानदारी की कलम,
वो जनता से जुड़ा दृष्टिकोण,
और वो संवेदना, जो एक सच्चे लेखक को समाज से जोड़ती है।
मैं चाहता हूँ कि मेरी इस आत्मकथा को पढ़कर कोई एक युवक यह कहे—
“मैं भी लिखूँगा, लेकिन सच्चाई के लिए।”
अगर ऐसा हुआ, तो मैं मानूंगा कि मेरी ज़िन्दगी सफल हुई।
आख़िर में, जब मैं जीवन के इस पड़ाव पर खड़ा हूँ, तो कोई अफ़सोस नहीं।
न धन का लोभ था, न प्रसिद्धि की भूख—बस एक प्यास थी कुछ कर गुजरने की, कुछ कहने की, और कुछ बदलने की।
और जब मेरी कलम रुकेगी, तो यकीन है कि कोई और हाथ उसे थाम लेगा…
क्योंकि सपने कभी मरते नहीं—वे पीढ़ी दर पीढ़ी ज़िंदा रहते हैं।
धन्यवाद ज्ञापन
(पृष्ठ संख्या – 44)
हर यात्रा अकेले पूरी नहीं होती।
यह आत्मकथा केवल मेरी नहीं है—यह उन सभी की साझी कहानी है जिन्होंने किसी न किसी रूप में मुझे संबल दिया, मार्ग दिखाया, और मेरी लेखनी को दिशा दी।
सबसे पहले, मैं अपने माता-पिता को नमन करता हूँ—जिनकी तपस्या, संस्कार और आशीर्वाद ने मुझे ज़मीन से जोड़े रखा, और आत्मबल से भरपूर किया।
बिबियापुर गाँव, जिसकी गलियों में मैंने जीवन का पहला पाठ पढ़ा, और जिन खेतों-खलिहानों में मैं बड़ा हुआ—वहाँ की मिट्टी और वहाँ के लोग मेरे जीवन की पहली पाठशाला रहे हैं।
मेरे शिक्षकों को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने शिक्षा के साथ-साथ सोचने का तरीका भी सिखाया, और हर मोड़ पर मुझे प्रेरणा दी।
मैं अपने पत्रकार साथियों, विशेष रूप से हिन्दी दैनिक आज, राष्ट्रीय सहारा, पंजाब केसरी, और अपराध टूडे के सहयोगियों का आभारी हूँ।जिन्होंने मेरी कलम को मंच दिया, और मेरी संवेदनाओं को पहचान दी।
संदेश महल की संपूर्ण टीम—संपादक, सहयोगी पत्रकार, तकनीकी साथी और पाठकों का दिल से आभार। आप सभी के बिना यह यात्रा अधूरी होती।
ह्यूमन वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के समस्त कार्यकर्ता, और लाभार्थी—जिनके साथ मैंने सेवा के क्षण बाँटे, उनका आभार, जिन्होंने मुझे एक बेहतर इंसान बनने का अवसर दिया।
मैं उन गुमनाम पाठकों का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जो मेरी किसी रचना को पढ़कर प्रेरित हुए, जिन्होंने कभी कोई चिठ्ठी लिखी, कोई संदेश भेजा, या चुपचाप किसी को मेरी लेखनी से जोड़ दिया।
अंत में, मैं इस आत्मकथा को पढ़ने वाले हर पाठक को धन्यवाद देता हूँ।अगर मेरे शब्दों में आपको अपने जीवन की झलक मिली,अगर मेरी यात्राओं ने आपके हौसले को छुआ तो यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है।
आपका –
जयप्रकाश रावत
संपादक, संदेश महल
संघर्ष से आत्मबोध तक
हर पथिक की यात्रा में कोई अंतिम मंज़िल नहीं होती — बस पड़ाव होते हैं, अनुभव होते हैं, और सीख होती है। मेरी यह आत्मकथा, मेरे जीवन की यात्रा का एक ऐसा ही पड़ाव है, जहाँ मैंने पीछे मुड़कर देखा और हर उस क्षण को जिया जिसने मुझे आज का ‘मैं’ बनाया।
यह आत्मकथा सिर्फ़ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की परतें हैं — जिनमें कभी भूख थी, कभी जुनून, कभी विद्रोह, और कहीं बहुत गहरा प्रेम — अपनी माटी से, अपनी मातृभाषा से, अपने लोगों से।
मैंने देखा है कि एक सच्ची आवाज़, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों न हो, अंततः सुनी जाती है। और अगर वह आवाज़ कलम से निकले, तो वह विचार बन जाती है — और विचार कभी मरते नहीं।
आज जब मैं यह लेखनी समेट रहा हूँ, तो कोई विराम नहीं लगाता — सिर्फ़ एक अल्पविराम छोड़ता हूँ। क्योंकि जीवन की असल किताब अब भी लिखी जा रही है — हर दिन, हर संघर्ष, हर शब्द से।
यह आत्मकथा अब आपकी है।आपके विचारों की, आपके सवालों की, आपके निर्णयों की।
मैंने अपने हिस्से की बात कह दी। अब आपकी बारी है…
– जयप्रकाश रावत
“मैं एक साधारण आदमी हूँ — पर मेरी कलम कभी साधारण नहीं रही।”
जयप्रकाश रावत
संस्थापक – संदेश महल
प्रेसीडेंट – ह्यूमन वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट
“मैंने जीवन जिया नहीं, उसे समझने की कोशिश की — और जो समझा, वही शब्दों में उतारा।”
आपका –
जयप्रकाश रावत
संस्थापक – संदेश महल
प्रेसीडेंट – ह्यूमन वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट
Email: sandeshmahal@gmail.com | www.sandeshmahal.com
प्रकाशकीय
“मेरी कलम, मेरा संघर्ष” केवल एक आत्मकथा नहीं, बल्कि एक दौर का दस्तावेज़ है—एक ऐसे पत्रकार की ज़िन्दगी का, जिसने न सत्ता का सहारा लिया, न प्रचार की चकाचौंध को अपनाया, बल्कि सत्य, संघर्ष और समाज को ही अपनी धुरी बनाया।
जयप्रकाश रावत जी की यह जीवन यात्रा गाँव की पगडंडी से शुरू होकर पत्रकारिता के राष्ट्रव्यापी मंच तक पहुँचती है, और फिर वहीं से लौटकर समाज की सेवा में समर्पित हो जाती है।यह पुस्तक पत्रकारिता, सामाजिक सरोकार और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं का वह संगम है, जो आज की पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बन सकता है।
यह आत्मकथा पाठक को भीतर तक छूती है, क्योंकि इसमें दिखावटी चमक नहीं, बल्कि ईमानदार सादगी है।यहाँ एक बच्चे की आँखों से दुनिया को देखना भी है, और एक अनुभवी कलमकार की सोच से व्यवस्था को परखना भी।साहित्यिक दृष्टि से देखें तो यह पुस्तक भाषा की सहजता, अनुभव की गहराई और संवेदना की ऊष्मा से भरी हुई है। लेखक ने जिस ईमानदारी से अपने जीवन के उतार-चढ़ाव, संघर्ष, हार-जीत और मन के भावों को उकेरा है, वह सराहनीय है।
प्रकाशन की प्रक्रिया के दौरान, यह स्पष्ट हुआ कि यह आत्मकथा न केवल एक व्यक्ति की कहानी है, बल्कि एक समाज की कहानी है—उस समाज की, जो बदलाव की उम्मीद में जी रहा है और सच्ची आवाज़ों की तलाश में है।
हमें गर्व है कि संदेश महल प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया। यह केवल लेखनी की यात्रा नहीं, बल्कि विश्वास की विजय है।
हम आशा करते हैं कि यह आत्मकथा पाठकों के दिल को छुएगी, सोच को जागृत करेगी, और शायद किसी युवा को यह कहने की प्रेरणा देगी—मैं भी सच्चाई की राह पर चलूँगा, मैं भी कलम उठाऊँगा!”